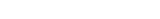Question:-1
Discuss the fundamental features of the Indian Constitution. How do these features shape the democratic character of the Indian state?
Answer:
🏛 Fundamental Features of the Indian Constitution and Their Role in Shaping Democracy
The Indian Constitution, adopted on 26 January 1950, serves as the supreme law of the land, providing a comprehensive framework for governance and safeguarding the rights of citizens. It reflects the aspirations of a diverse nation and ensures the establishment of a sovereign, socialist, secular, and democratic republic. Its fundamental features play a pivotal role in maintaining the democratic ethos of the country.
1. 📝 Written and Lengthy Constitution
The Indian Constitution is one of the lengthiest written constitutions in the world, containing 448 articles, 12 schedules, and numerous amendments. This detail ensures clarity on the powers, functions, and limitations of various organs of the government.
- Impact on Democracy: Its detailed nature minimizes ambiguities, promotes transparency, and ensures citizens' participation in governance through well-defined rights and duties.
2. ⚖️ Supremacy of the Constitution
The Constitution holds the highest legal authority in India. All laws, rules, and actions of the government must conform to its provisions. The judiciary has the power of judicial review to strike down unconstitutional acts.
- Impact on Democracy: This ensures that no individual or institution can act above the law, maintaining rule of law, a cornerstone of democracy.
3. 📜 Fundamental Rights and Duties
Part III of the Constitution guarantees Fundamental Rights such as equality, freedom of speech, and protection against exploitation. Part IV-A outlines Fundamental Duties, encouraging responsible citizenship.
- Example: The Right to Equality prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth.
- Impact on Democracy: These provisions empower citizens and promote an inclusive and participatory democracy by safeguarding individual liberties.
4. 🗳 Parliamentary System of Government
India follows a parliamentary democracy based on the Westminster model, where the executive is accountable to the legislature. The Prime Minister and Council of Ministers are collectively responsible to the Lok Sabha.
- Impact on Democracy: This system ensures collective responsibility and accountability, reflecting the will of the people.
5. 🌍 Federal Structure with a Unitary Bias
India has a federal framework with powers divided between the Union and the States (Union List, State List, Concurrent List). However, in times of emergency, the Constitution allows the Centre to assume greater control.
- Impact on Democracy: It balances unity and diversity, accommodating regional aspirations while preserving national integrity.
6. ⚖️ Independent Judiciary
The judiciary, headed by the Supreme Court, is independent of the executive and legislature. It safeguards the Constitution through its power of judicial review.
- Impact on Democracy: Ensures protection of citizens’ rights and prevents misuse of power by other organs of the state.
7. 📚 Directive Principles of State Policy (DPSPs)
Though not justiciable, DPSPs guide the government in creating policies to achieve social and economic justice. They reflect the ideal of a welfare state.
- Example: Provisions for promoting equal pay for equal work and improving public health.
- Impact on Democracy: They ensure that democracy is not limited to political equality but extends to social and economic dimensions.
8. 🌐 Secularism
India is a secular state, meaning the government maintains neutrality towards all religions and does not establish any state religion.
- Impact on Democracy: Protects the rights of minorities and promotes religious harmony, a key aspect of a diverse democracy.
9. ✍ Amending Procedure
The Constitution provides for amendments (Article 368), making it neither too rigid nor too flexible.
- Impact on Democracy: This adaptability allows the Constitution to evolve with changing times while safeguarding core democratic principles.
🏆 Conclusion
The fundamental features of the Indian Constitution form the backbone of its democratic character. By ensuring rule of law, equality, accountability, and participation, they create a framework where citizens are both the source and beneficiaries of power. Through a blend of flexibility and stability, the Constitution has successfully guided India in maintaining its democratic ideals while accommodating its vast social, cultural, and political diversity.
Question:-2
Explain the composition and powers of the Parliament of India. How does it ensure the executive's accountability?
Answer:
🏛 Composition and Powers of the Parliament of India: Ensuring Executive Accountability
The Parliament of India serves as the supreme legislative authority of the nation and plays a crucial role in shaping its democratic framework. Established under Part V of the Indian Constitution, it is responsible for law-making, representing the people, and holding the executive accountable.
1. 🧩 Composition of the Parliament of India
The Indian Parliament comprises two houses along with the President of India, making it a bicameral legislature.
a) The President
- The President is an integral part of Parliament (Article 79) and performs legislative functions such as summoning and proroguing sessions, giving assent to bills, and addressing Parliament at the commencement of the first session each year.
b) Lok Sabha (House of the People)
- Members are directly elected by the people through universal adult suffrage.
- The maximum strength is 552 members (530 from States, 20 from Union Territories, and 2 nominated by the President from the Anglo-Indian community if necessary).
- The tenure is five years, but it may be dissolved earlier.
c) Rajya Sabha (Council of States)
- It is a permanent body that is not subject to dissolution, with one-third of its members retiring every two years.
- The maximum strength is 250 members (238 elected by State and Union Territory legislatures, 12 nominated by the President for contributions to arts, science, literature, and social service).
- Members are elected by indirect voting through proportional representation by a single transferable vote.
2. ⚖️ Powers of the Parliament of India
The Parliament wields extensive powers that cover various domains, ensuring the smooth functioning of the democratic system.
a) Legislative Powers
- The Parliament makes laws on Union List and Concurrent List subjects (Article 246).
- In exceptional cases, it can also legislate on State List matters during a national emergency (Article 249, 250).
- Example: Enacting the Goods and Services Tax (GST) law by amending the Constitution.
b) Financial Powers
- The Parliament controls public finances through the annual budget.
- No money can be withdrawn from the Consolidated Fund of India without its approval.
- The Lok Sabha enjoys greater financial powers, as Money Bills can only originate here (Article 110).
c) Executive Powers
- The Council of Ministers, headed by the Prime Minister, is collectively responsible to the Lok Sabha (Article 75).
- Parliament can remove the Council through a no-confidence motion.
d) Judicial Powers
- It has the power to impeach the President (Article 61).
- It can also remove judges of the Supreme Court and High Courts for proven misconduct or incapacity.
e) Electoral Powers
- Members of Parliament participate in the election of the President and Vice President.
f) Amending Powers
- Under Article 368, Parliament can amend the Constitution, except for provisions that form its basic structure.
3. 🧭 How Parliament Ensures Executive Accountability
One of the Parliament’s most vital roles is to ensure the executive functions transparently and responsibly.
- Question Hour & Zero Hour: Ministers answer questions posed by MPs, enabling scrutiny of government actions.
- Debates and Discussions: Policies and bills are debated, allowing members to voice concerns and influence decisions.
- No-Confidence Motion: If the government loses the confidence of the Lok Sabha, it must resign.
- Parliamentary Committees: Committees such as the Public Accounts Committee (PAC) and Estimates Committee examine government expenditure and policies.
- Censure Motions and Adjournment Motions: These allow MPs to express dissatisfaction with specific actions or policies of the government.
Through these mechanisms, the executive remains accountable to the legislature, ensuring that power is exercised within constitutional limits and in the interest of the people.
🏆 Conclusion
The Indian Parliament, with its bicameral structure, extensive powers, and well-defined procedures, plays a central role in maintaining the democratic essence of the nation. Its ability to legislate, control finances, and scrutinize the executive ensures a balance of power, preventing authoritarianism. By upholding transparency, accountability, and representation, the Parliament remains the cornerstone of India’s democratic governance.
Question:-3
Examine the role and powers of the President of India in a parliamentary system.
Answer:
🇮🇳 Role and Powers of the President of India in a Parliamentary System
The President of India serves as the constitutional head of the state and represents the unity of the nation. Positioned as the ceremonial head, the President functions within the framework of a parliamentary system, where the real executive power lies with the Council of Ministers headed by the Prime Minister (Article 74).
1. 👤 Role of the President
a) Constitutional Head
The President performs functions as per the advice of the Council of Ministers, ensuring the smooth operation of the parliamentary system.
b) Symbol of Unity and Integrity
The President represents the nation both domestically and internationally, upholding the dignity of the Republic.
c) Guardian of the Constitution
As the supreme constitutional authority, the President ensures that all organs of government act within constitutional limits.
2. ⚖️ Powers of the President
a) Executive Powers
- Appoints the Prime Minister, Council of Ministers, Governors, Chief Justices, and Ambassadors.
- Exercises control over Union Territories and is the supreme commander of the armed forces.
b) Legislative Powers
- Summons, prorogues, and dissolves Parliament.
- Gives assent to bills and can return non-money bills for reconsideration (Article 111).
- Issues ordinances (Article 123) when Parliament is not in session.
c) Financial Powers
- Causes the Union Budget to be laid before Parliament.
- Ensures no money bill is introduced without prior recommendation.
d) Judicial Powers
- Exercises the power to grant pardons, reprieves, respites, or remissions (Article 72).
e) Emergency Powers
- Can declare national, state, or financial emergencies under Articles 352, 356, and 360.
🏆 Conclusion
The President of India plays a vital constitutional and ceremonial role within the parliamentary system. While the office is largely nominal, the President acts as a safeguard against constitutional crises, ensures continuity in governance, and upholds democratic values by acting on the advice of the Council of Ministers while retaining certain discretionary powers in exceptional situations.
Question:-4
What do you understand by the concept of constitutionalism? How is it reflected in India’s constitutional structure?
Answer:
📜 Concept of Constitutionalism and Its Reflection in India
Understanding Constitutionalism
Constitutionalism refers to the principle that the authority of the government is derived from and limited by a body of fundamental laws or a constitution. It emphasizes limited government, rule of law, separation of powers, and protection of individual rights. The concept ensures that no branch of government acts beyond its constitutional mandate, thereby preventing arbitrary use of power.
Key Features of Constitutionalism
- Supremacy of the Constitution – The constitution is the highest law, and all organs of government must act in accordance with it.
- Rule of Law – Everyone, including lawmakers and the executive, is subject to the same laws.
- Fundamental Rights – Guarantees individual freedoms and liberties against state encroachment.
- Checks and Balances – Ensures that power is distributed and regulated among different branches of government.
Reflection of Constitutionalism in India
India’s Constitution, adopted in 1950, is a written and supreme document that embodies the ideals of constitutionalism. Its provisions reflect this concept in multiple ways:
- Division of Powers: It establishes a federal structure with clear separation between the Union and States (Seventh Schedule).
- Fundamental Rights (Part III): Safeguards individual freedoms such as equality (Article 14) and freedom of speech (Article 19).
- Judicial Review (Articles 13 & 32): The Supreme Court and High Courts ensure laws comply with constitutional provisions.
- Directive Principles (Part IV): Guide the state in promoting social and economic justice while adhering to constitutional limits.
- Amendment Process (Article 368): Allows flexibility but protects the basic structure, as upheld in the Kesavananda Bharati case (1973).
Conclusion
Constitutionalism in India ensures that governance operates within defined boundaries, protecting democracy and individual rights while preventing authoritarian tendencies. Its reflection lies in the balance between flexibility and restraint, allowing evolution without compromising constitutional supremacy.
Question:-5
Describe the federal features of the Indian Constitution. In what ways is Indian federalism unique?
Answer:
🌏 Federal Features of the Indian Constitution and Its Unique Nature
Federal Features of the Indian Constitution
The Indian Constitution incorporates several features of a federal system, ensuring a division of powers between the Union and the States. Key federal aspects include:
- Division of Powers (Seventh Schedule): Subjects are divided into Union, State, and Concurrent Lists, clearly outlining legislative jurisdiction.
- Written and Supreme Constitution: It is a detailed document that acts as the highest law, binding on both Union and States.
- Independent Judiciary: The Supreme Court serves as the guardian of the Constitution and resolves disputes between the Centre and States (Article 131).
- Dual Government Polity: It establishes two levels of government—central and state—with separate responsibilities.
- Bicameral Legislature: Rajya Sabha represents the states at the national level, ensuring their participation in law-making.
Unique Nature of Indian Federalism
Indian federalism is often described as “federal in form but unitary in spirit.” Unlike classical federations such as the USA, it exhibits a strong centralizing tendency, making it distinctive.
- Single Citizenship: Unlike some federations, Indian citizens enjoy only one citizenship, emphasizing unity.
- Emergency Provisions (Articles 352, 356, 360): During emergencies, the Centre assumes greater powers, reducing state autonomy.
- Residuary Powers (Article 248): These are vested in the Union, ensuring a strong central authority.
- Unified Judiciary and Election Machinery: Both are centralized to maintain uniformity across states.
- Flexibility of the Constitution: Certain amendments require only a simple majority of Parliament, reflecting a unitary tilt.
Conclusion
The Indian Constitution establishes a federal framework tailored to its diversity and historical context, yet ensures national integration through strong central features. This quasi-federal model balances state autonomy with the need for a unified and stable governance structure.
Question:-6
What is the significance of the Preamble to the Indian Constitution?
Answer:
📜 Significance of the Preamble to the Indian Constitution
The Preamble of the Indian Constitution serves as its philosophical guide and essence, reflecting the vision of the framers and the aspirations of the people. It declares India to be a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic, emphasizing key objectives such as Justice (social, economic, and political), Liberty (of thought, expression, belief, faith, and worship), Equality (of status and opportunity), and Fraternity (assuring dignity and unity).
Its significance lies in providing the foundation of constitutional values and acting as a source of authority, affirming that power rests with the people. Though not legally enforceable, it plays a vital role in guiding the judiciary during constitutional interpretation, as upheld in the Kesavananda Bharati case (1973). Furthermore, it promotes national unity and integrity by fostering fraternity and dignity among citizens. Thus, the Preamble is both an introductory statement and a moral compass for Indian democracy.
Question:-7
Write a short note on the role of the Election Commission of India.
Answer:
🗳 Role of the Election Commission of India
The Election Commission of India (ECI) is an autonomous constitutional body established under Article 324 to administer and oversee free and fair elections in the country. It is responsible for conducting elections to the Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislatures, and the offices of the President and Vice-President.
The Commission ensures the implementation of the Model Code of Conduct, monitors election expenditure, and supervises the nomination process, voting, and counting of votes. It also regulates political parties, grants recognition, and allots election symbols.
The ECI plays a critical role in strengthening democracy by ensuring transparency, impartiality, and inclusiveness in the electoral process. Its powers include advising on disqualification of candidates, enforcing election laws, and ordering re-polls when necessary.
Through its functions, the Election Commission safeguards the principle of universal adult suffrage and upholds the credibility of India’s democratic framework.
Question:-8
Define the concept of judicial review.
Answer:
⚖️ Concept of Judicial Review
Judicial review refers to the power of the judiciary to examine the constitutionality of laws, executive orders, and legislative actions. It ensures that all organs of government act within the limits prescribed by the Constitution. In India, this concept is derived primarily from Articles 13, 32, and 226, empowering the Supreme Court and High Courts to declare any law or action void if it violates fundamental rights or the basic structure of the Constitution.
Judicial review acts as a safeguard against arbitrary governance, protecting citizens' rights and maintaining the supremacy of the Constitution. Landmark judgments, such as the Kesavananda Bharati case (1973), reaffirmed that Parliament cannot alter the basic structure of the Constitution through amendments.
Thus, judicial review is a cornerstone of Indian democracy, ensuring checks and balances among the legislature, executive, and judiciary while upholding the principles of rule of law and constitutional supremacy.
Question:-9
Mention any four Directive Principles of State Policy and their importance.
Answer:
🏛 Four Directive Principles of State Policy and Their Importance
The Directive Principles of State Policy (DPSPs), enshrined in Part IV of the Indian Constitution (Articles 36–51), guide the government in creating policies aimed at achieving a just and equitable society. They are non-justiciable but hold significant moral and political value.
Four Key Directive Principles
- Right to adequate means of livelihood (Article 39) – Ensures fair distribution of resources and opportunities for all citizens.
- Equal pay for equal work (Article 39(d)) – Promotes gender equality and fair labor practices.
- Provision for free and compulsory education for children (Article 45) – Strengthens the foundation of education and social development.
- Promotion of health and nutrition (Article 47) – Aims to improve public health and raise living standards.
Importance
DPSPs act as a guiding framework for governance, aiming to establish a welfare state. They influence legislation, reduce inequality, and promote social and economic justice, complementing Fundamental Rights to ensure holistic development.
Question:-10
How are Fundamental Duties linked with ethical values?
Answer:
🌟 Link Between Fundamental Duties and Ethical Values
Fundamental Duties, introduced by the 42nd Amendment of the Indian Constitution (1976) under Article 51A, outline the moral responsibilities of citizens towards the nation. They serve as a guide for ethical conduct, complementing Fundamental Rights to create a balanced civic framework.
These duties promote values such as patriotism, respect for the Constitution, social harmony, environmental protection, and scientific temper. For instance, the duty to safeguard public property encourages honesty and civic responsibility, while promoting harmony and respecting diversity fosters tolerance and empathy.
By internalizing these duties, citizens develop a sense of moral obligation and social responsibility, which goes beyond legal compliance. They act as ethical benchmarks for behavior in daily life, reinforcing democratic ideals, justice, and national integrity.
Thus, Fundamental Duties serve as a bridge between law and morality, guiding citizens to act responsibly, uphold social values, and contribute positively to nation-building.
प्रश्न:-1
भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ये विशेषताएँ भारतीय राज्य के लोकतांत्रिक चरित्र को किस प्रकार आकार देती हैं?
उत्तर:
🏛 भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं और लोकतंत्र को आकार देने में उनकी भूमिका
26 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारतीय संविधान, देश के सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है, जो शासन के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह एक विविध राष्ट्र की आकांक्षाओं को दर्शाता है और एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना सुनिश्चित करता है । इसकी मूलभूत विशेषताएँ देश के लोकतांत्रिक लोकाचार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
1. 📝 लिखित और लंबा संविधान
भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है , जिसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और कई संशोधन शामिल हैं । यह विवरण सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों, कार्यों और सीमाओं पर स्पष्टता सुनिश्चित करता है।
- लोकतंत्र पर प्रभाव: इसकी विस्तृत प्रकृति अस्पष्टताओं को कम करती है, पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, तथा सुपरिभाषित अधिकारों और कर्तव्यों के माध्यम से शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करती है।
2. ⚖️ संविधान की सर्वोच्चता
भारत में संविधान सर्वोच्च कानूनी अधिकार रखता है। सरकार के सभी कानून, नियम और कार्य इसके प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए। न्यायपालिका के पास असंवैधानिक कृत्यों को रद्द करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति है।
- लोकतंत्र पर प्रभाव: यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर कार्य नहीं कर सकती, तथा कानून का शासन , जो लोकतंत्र की आधारशिला है, को बनाए रखता है।
3. 📜 मौलिक अधिकार और कर्तव्य
संविधान का भाग III समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शोषण से सुरक्षा जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। भाग IV-A मौलिक कर्तव्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है , जो ज़िम्मेदार नागरिकता को प्रोत्साहित करता है।
- उदाहरण: समानता का अधिकार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।
- लोकतंत्र पर प्रभाव: ये प्रावधान नागरिकों को सशक्त बनाते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करके समावेशी और सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं।
4. 🗳 संसदीय शासन प्रणाली
भारत वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र का पालन करता है , जहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- लोकतंत्र पर प्रभाव: यह प्रणाली लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित करते हुए सामूहिक जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
5. 🌍 एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय संरचना
भारत में एक संघीय ढाँचा है जिसमें शक्तियाँ संघ और राज्यों (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची) के बीच विभाजित हैं। हालाँकि, आपातकाल के समय, संविधान केंद्र को अधिक नियंत्रण संभालने की अनुमति देता है।
- लोकतंत्र पर प्रभाव: यह एकता और विविधता में संतुलन स्थापित करता है, राष्ट्रीय अखंडता को संरक्षित करते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करता है।
6. ⚖️ स्वतंत्र न्यायपालिका
सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। यह न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति के माध्यम से संविधान की रक्षा करती है।
- लोकतंत्र पर प्रभाव: नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और राज्य के अन्य अंगों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है।
7. 📚 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी)
यद्यपि न्यायोचित नहीं, डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए नीतियाँ बनाने में सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। वे एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्रतिबिम्बित करते हैं ।
- उदाहरण: समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के प्रावधान।
- लोकतंत्र पर प्रभाव: वे यह सुनिश्चित करते हैं कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता तक सीमित न रहे बल्कि सामाजिक और आर्थिक आयामों तक फैले ।
8. 🌐 धर्मनिरपेक्षता
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि सरकार सभी धर्मों के प्रति तटस्थता बनाए रखती है और कोई भी राज्य धर्म स्थापित नहीं करती है।
- लोकतंत्र पर प्रभाव: अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देता है , जो कि विविधतापूर्ण लोकतंत्र का एक प्रमुख पहलू है।
9. ✍ संशोधन प्रक्रिया
संविधान में संशोधन का प्रावधान है (अनुच्छेद 368) , जिससे यह न तो बहुत कठोर है और न ही बहुत लचीला।
- लोकतंत्र पर प्रभाव: यह अनुकूलनशीलता संविधान को बदलते समय के साथ विकसित होने की अनुमति देती है, जबकि मूल लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा भी होती है।
🏆 निष्कर्ष
भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएँ इसके लोकतांत्रिक चरित्र की रीढ़ हैं । कानून का शासन, समानता, जवाबदेही और भागीदारी सुनिश्चित करके , ये विशेषताएँ एक ऐसा ढाँचा तैयार करती हैं जहाँ नागरिक सत्ता के स्रोत और लाभार्थी दोनों होते हैं। लचीलेपन और स्थिरता के मिश्रण के माध्यम से, संविधान ने भारत की विशाल सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता को समायोजित करते हुए, उसके लोकतांत्रिक आदर्शों को बनाए रखने में सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया है।
प्रश्न:-2
भारतीय संसद की संरचना और शक्तियों की व्याख्या कीजिए। यह कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है?
उत्तर:
🏛 भारतीय संसद की संरचना और शक्तियाँ: कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करना
भारत की संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है और इसके लोकतांत्रिक ढाँचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय संविधान के भाग V के अंतर्गत स्थापित , यह कानून बनाने, जनता का प्रतिनिधित्व करने और कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने के लिए ज़िम्मेदार है।
1. 🧩 भारत की संसद की संरचना
भारतीय संसद में भारत के राष्ट्रपति सहित दो सदन होते हैं , जिससे यह द्विसदनीय विधायिका बन जाती है।
क) राष्ट्रपति
- राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है (अनुच्छेद 79) और वह विधायी कार्य करता है, जैसे सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना , विधेयकों को स्वीकृति देना , तथा प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद को संबोधित करना।
ख) लोकसभा (लोक सभा)
- सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से जनता द्वारा सीधे किया जाता है।
- अधिकतम सदस्य संख्या 552 है (530 राज्यों से, 20 संघ शासित प्रदेशों से, तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय से, यदि आवश्यक हो तो, मनोनीत)।
- इसका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है , लेकिन इसे पहले भी भंग किया जा सकता है।
ग) राज्य सभा (राज्य परिषद)
- यह एक स्थायी निकाय है जो कभी विघटित नहीं होता, तथा इसके एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
- अधिकतम सदस्य संख्या 250 है (238 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित, 12 राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक सेवा में योगदान के लिए नामित)।
- सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।
2. ⚖️ भारत की संसद की शक्तियाँ
संसद के पास व्यापक शक्तियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों को कवर करती हैं, तथा लोकतांत्रिक प्रणाली के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करती हैं।
क) विधायी शक्तियाँ
- संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है (अनुच्छेद 246)।
- असाधारण मामलों में, यह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के मामलों पर भी कानून बना सकता है (अनुच्छेद 249, 250) ।
- उदाहरण: संविधान में संशोधन करके वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून बनाना।
ख) वित्तीय शक्तियां
- संसद वार्षिक बजट के माध्यम से सार्वजनिक वित्त को नियंत्रित करती है ।
- भारत की समेकित निधि से उसकी स्वीकृति के बिना कोई धनराशि नहीं निकाली जा सकती।
- लोक सभा को अधिक वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि धन विधेयक केवल यहीं से पारित हो सकते हैं (अनुच्छेद 110)।
ग) कार्यकारी शक्तियाँ
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है (अनुच्छेद 75)।
- संसद अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से परिषद को हटा सकती है ।
घ) न्यायिक शक्तियां
- इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति है (अनुच्छेद 61) ।
- यह सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी हटा सकता है।
ई) चुनावी शक्तियां
- संसद सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं ।
च) संशोधन शक्तियां
- अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, सिवाय उन प्रावधानों के जो इसके मूल ढांचे का निर्माण करते हैं।
3. 🧭 संसद कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है
संसद की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक यह सुनिश्चित करना है कि कार्यपालिका पारदर्शी और जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करे ।
- प्रश्नकाल और शून्यकाल: मंत्री सांसदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे सरकारी कार्यों की जांच संभव हो पाती है।
- वाद-विवाद और चर्चाएं: नीतियों और विधेयकों पर बहस की जाती है, जिससे सदस्यों को अपनी चिंताएं व्यक्त करने और निर्णयों को प्रभावित करने का अवसर मिलता है।
- अविश्वास प्रस्ताव: यदि सरकार लोकसभा का विश्वास खो देती है, तो उसे इस्तीफा देना होगा।
- संसदीय समितियाँ: लोक लेखा समिति (पीएसी) और प्राक्कलन समिति जैसी समितियाँ सरकारी व्यय और नीतियों की जांच करती हैं।
- निंदा प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव: ये सांसदों को सरकार के विशिष्ट कार्यों या नीतियों के प्रति असंतोष व्यक्त करने की अनुमति देते हैं।
इन तंत्रों के माध्यम से, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह बनी रहती है , तथा यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता का प्रयोग संवैधानिक सीमाओं के भीतर और लोगों के हित में किया जाए।
🏆 निष्कर्ष
भारतीय संसद, अपनी द्विसदनीय संरचना, व्यापक शक्तियों और सुस्पष्ट प्रक्रियाओं के साथ , राष्ट्र के लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखने में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। कानून बनाने, वित्त पर नियंत्रण और कार्यपालिका की जाँच करने की इसकी क्षमता शक्ति संतुलन सुनिश्चित करती है और अधिनायकवाद को रोकती है। पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रतिनिधित्व को कायम रखते हुए , संसद भारत के लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला बनी हुई है।
प्रश्न:-3
संसदीय प्रणाली में भारत के राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियों का परीक्षण करें।
उत्तर:
🇮🇳 संसदीय प्रणाली में भारत के राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियाँ
भारत का राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राष्ट्र की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। औपचारिक प्रमुख के रूप में , राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली के ढांचे के भीतर कार्य करता है , जहाँ वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है (अनुच्छेद 74)।
1. 👤 राष्ट्रपति की भूमिका
क) संवैधानिक प्रमुख
राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, जिससे संसदीय प्रणाली का सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है।
ख) एकता और अखंडता का प्रतीक
राष्ट्रपति गणतंत्र की गरिमा को बनाए रखते हुए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है।
c) संविधान का संरक्षक
सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में, राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के सभी अंग संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करें।
2. ⚖️ राष्ट्रपति की शक्तियाँ
क) कार्यकारी शक्तियां
- प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों और राजदूतों की नियुक्ति करता है।
- संघ शासित प्रदेशों पर नियंत्रण रखता है तथा सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है।
ख) विधायी शक्तियाँ
- संसद को बुलाना, स्थगित करना और भंग करना।
- विधेयकों को स्वीकृति देता है तथा गैर-धन विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है (अनुच्छेद 111)।
- जब संसद सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी करना (अनुच्छेद 123) ।
ग) वित्तीय शक्तियां
- केन्द्रीय बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- यह सुनिश्चित किया जाता है कि बिना पूर्व सिफारिश के कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत न किया जाए।
घ) न्यायिक शक्तियां
- क्षमा, प्रविलंब, विराम या छूट देने की शक्ति का प्रयोग करता है (अनुच्छेद 72)।
ई) आपातकालीन शक्तियां
- अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ।
🏆 निष्कर्ष
भारत के राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और औपचारिक भूमिका निभाते हैं। हालाँकि यह पद नाममात्र का होता है, राष्ट्रपति संवैधानिक संकटों से सुरक्षा प्रदान करते हैं , शासन में निरंतरता सुनिश्चित करते हैं, और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हुए, असाधारण परिस्थितियों में कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ अपने पास रखते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हैं।
प्रश्न:-4
संविधानवाद की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? यह भारत के संवैधानिक ढांचे में कैसे परिलक्षित होता है?
उत्तर:
📜 संविधानवाद की अवधारणा और भारत में इसका प्रतिबिंब
संविधानवाद को समझना
संविधानवाद उस सिद्धांत को संदर्भित करता है जिसके अनुसार सरकार का अधिकार मौलिक कानूनों या संविधान के एक समूह से प्राप्त और सीमित होता है। यह सीमित सरकार, कानून के शासन, शक्तियों के पृथक्करण और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण पर ज़ोर देता है । यह अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि सरकार की कोई भी शाखा अपने संवैधानिक अधिदेश से परे कार्य न करे, जिससे सत्ता के मनमाने इस्तेमाल को रोका जा सके।
संविधानवाद की प्रमुख विशेषताएं
- संविधान की सर्वोच्चता - संविधान सर्वोच्च कानून है, और सरकार के सभी अंगों को इसके अनुसार कार्य करना चाहिए।
- कानून का शासन - कानून निर्माता और कार्यपालिका सहित सभी लोग समान कानून के अधीन हैं।
- मौलिक अधिकार - राज्य के अतिक्रमण के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतन्त्रता की गारंटी देता है।
- नियंत्रण और संतुलन - यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति वितरित और विनियमित हो।
भारत में संविधानवाद का प्रतिबिंब
1950 में अपनाया गया भारत का संविधान एक लिखित और सर्वोच्च दस्तावेज़ है जो संविधानवाद के आदर्शों को मूर्त रूप देता है। इसके प्रावधान इस अवधारणा को कई तरह से दर्शाते हैं:
- शक्तियों का विभाजन: यह संघ और राज्यों के बीच स्पष्ट पृथक्करण के साथ एक संघीय ढांचे की स्थापना करता है (सातवीं अनुसूची)।
- मौलिक अधिकार (भाग III): समानता (अनुच्छेद 14) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) जैसी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है।
- न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 13 और 32): सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि कानून संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हों।
- नीति निर्देशक सिद्धांत (भाग IV): संवैधानिक सीमाओं का पालन करते हुए सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने में राज्य का मार्गदर्शन करना।
- संशोधन प्रक्रिया (अनुच्छेद 368): लचीलेपन की अनुमति देता है लेकिन मूल संरचना की रक्षा करता है, जैसा कि केशवानंद भारती मामले (1973) में बरकरार रखा गया था।
निष्कर्ष
भारत में संविधानवाद यह सुनिश्चित करता है कि शासन निर्धारित सीमाओं के भीतर संचालित हो, लोकतंत्र और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हुए सत्तावादी प्रवृत्तियों को रोके। इसकी झलक लचीलेपन और संयम के बीच संतुलन में निहित है , जो संवैधानिक सर्वोच्चता से समझौता किए बिना विकास की अनुमति देता है।
प्रश्न:-5
भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संघवाद किन मायनों में अद्वितीय है?
उत्तर:
🌏 भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं और इसकी विशिष्ट प्रकृति
भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएँ
भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की कई विशेषताएँ समाहित हैं, जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन सुनिश्चित करती हैं । प्रमुख संघीय पहलुओं में शामिल हैं:
- शक्तियों का विभाजन (सातवीं अनुसूची): विषयों को संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में विभाजित किया गया है, जो विधायी क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।
- लिखित एवं सर्वोच्च संविधान: यह एक विस्तृत दस्तावेज है जो सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है तथा संघ एवं राज्यों दोनों पर बाध्यकारी है।
- स्वतंत्र न्यायपालिका: सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करता है (अनुच्छेद 131)।
- दोहरी सरकार की राजनीति: यह सरकार के दो स्तर स्थापित करती है - केंद्रीय और राज्य - जिनकी अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं।
- द्विसदनीय विधानमंडल: राज्यसभा राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तथा कानून निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करती है।
भारतीय संघवाद की अनूठी प्रकृति
भारतीय संघवाद को अक्सर "रूप में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक" के रूप में वर्णित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पारंपरिक संघों के विपरीत, यह एक प्रबल केंद्रीकरण प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है , जो इसे विशिष्ट बनाता है।
- एकल नागरिकता: कुछ संघों के विपरीत, भारतीय नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्राप्त है, जो एकता पर बल देता है।
- आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352, 356, 360): आपातकाल के दौरान, केंद्र अधिक शक्तियां ग्रहण कर लेता है, जिससे राज्य की स्वायत्तता कम हो जाती है।
- अवशिष्ट शक्तियां (अनुच्छेद 248): ये संघ में निहित हैं, जो एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण सुनिश्चित करती हैं।
- एकीकृत न्यायपालिका और चुनाव मशीनरी: दोनों को राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए केंद्रीकृत किया गया है।
- संविधान का लचीलापन: कुछ संशोधनों के लिए संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जो एकात्मक झुकाव को दर्शाता है।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान अपनी विविधता और ऐतिहासिक संदर्भ के अनुरूप एक संघीय ढाँचा स्थापित करता है , साथ ही मज़बूत केंद्रीय विशेषताओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण सुनिश्चित करता है। यह अर्ध-संघीय मॉडल राज्य की स्वायत्तता और एक एकीकृत एवं स्थिर शासन संरचना की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करता है।
प्रश्न:-6
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है?
उत्तर:
📜 भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व
भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसके दार्शनिक मार्गदर्शक और सार के रूप में कार्य करती है , जो इसके निर्माताओं के दृष्टिकोण और जन आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करती है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) , स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की) , समानता (प्रतिष्ठा और अवसर की) और बंधुत्व (गरिमा और एकता का आश्वासन) जैसे प्रमुख उद्देश्यों पर बल देती है ।
इसका महत्व संवैधानिक मूल्यों की नींव रखने और अधिकार के स्रोत के रूप में कार्य करने में निहित है , जो इस बात की पुष्टि करता है कि सत्ता जनता के पास है। हालाँकि यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, फिर भी यह संवैधानिक व्याख्या के दौरान न्यायपालिका का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसा कि केशवानंद भारती मामले (1973) में कहा गया है । इसके अलावा, यह नागरिकों के बीच बंधुत्व और सम्मान को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देती है । इस प्रकार, प्रस्तावना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक परिचयात्मक कथन और एक नैतिक दिशानिर्देश दोनों है।
प्रश्न:-7
भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:
🗳 भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संचालन और निगरानी हेतु अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है । यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है ।
आयोग आदर्श आचार संहिता का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है , चुनाव व्यय की निगरानी करता है, नामांकन प्रक्रिया, मतदान और मतगणना का पर्यवेक्षण करता है। यह राजनीतिक दलों का विनियमन, मान्यता प्रदान करना और चुनाव चिह्न आवंटित करना भी करता है।
चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समावेशिता सुनिश्चित करके लोकतंत्र को मज़बूत बनाने में चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है । इसकी शक्तियों में उम्मीदवारों की अयोग्यता पर सलाह देना, चुनाव कानूनों को लागू करना और आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मतदान का आदेश देना शामिल है।
अपने कार्यों के माध्यम से, चुनाव आयोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत की रक्षा करता है और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की विश्वसनीयता को बनाए रखता है।
प्रश्न:-8
न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को परिभाषित करें।
उत्तर:
⚖️ न्यायिक समीक्षा की अवधारणा
न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की उस शक्ति को संदर्भित करती है जिसके द्वारा वह कानूनों, कार्यकारी आदेशों और विधायी कार्यों की संवैधानिकता की जाँच करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकार के सभी अंग संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करें। भारत में, यह अवधारणा मुख्यतः अनुच्छेद 13, 32 और 226 से ली गई है , जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को किसी भी कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित करने का अधिकार देती है यदि वह मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है।
न्यायिक समीक्षा मनमाने शासन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है। केशवानंद भारती मामले (1973) जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने इस बात की पुष्टि की कि संसद संशोधनों के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती।
इस प्रकार, न्यायिक समीक्षा भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, जो कानून के शासन और संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांतों को कायम रखते हुए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करती है ।
प्रश्न:-9
राज्य नीति के किन्हीं चार निर्देशक सिद्धांतों और उनके महत्व का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
🏛 राज्य नीति के चार निर्देशक सिद्धांत और उनका महत्व
भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) , एक न्यायसंगत और समतामूलक समाज के निर्माण हेतु नीतियाँ बनाने में सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। ये न्यायसंगत नहीं हैं, लेकिन इनका नैतिक और राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है।
चार प्रमुख निर्देशक सिद्धांत
- आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार (अनुच्छेद 39) - सभी नागरिकों के लिए संसाधनों और अवसरों का उचित वितरण सुनिश्चित करता है।
- समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39(डी)) - लैंगिक समानता और निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
- बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान (अनुच्छेद 45) – शिक्षा एवं सामाजिक विकास की नींव को मजबूत करता है।
- स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 47) - इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।
महत्त्व
डीपीएसपी शासन के लिए एक मार्गदर्शक ढाँचे के रूप में कार्य करते हैं , जिसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है । वे कानून को प्रभावित करते हैं, असमानता को कम करते हैं, और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं , तथा समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों के पूरक होते हैं।
प्रश्न:-10
मौलिक कर्तव्य नैतिक मूल्यों से किस प्रकार जुड़े हैं?
उत्तर:
🌟 मौलिक कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों के बीच संबंध
भारतीय संविधान के 42वें संशोधन (1976) द्वारा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत प्रस्तुत मौलिक कर्तव्य , राष्ट्र के प्रति नागरिकों की नैतिक ज़िम्मेदारियों को रेखांकित करते हैं। ये नैतिक आचरण के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और एक संतुलित नागरिक ढाँचा बनाने हेतु मौलिक अधिकारों के पूरक हैं।
ये कर्तव्य देशभक्ति, संविधान के प्रति सम्मान, सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक सोच जैसे मूल्यों को बढ़ावा देते हैं । उदाहरण के लिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य ईमानदारी और नागरिक ज़िम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है, जबकि सद्भाव को बढ़ावा देना और विविधता का सम्मान करना सहिष्णुता और सहानुभूति को बढ़ावा देता है।
इन कर्तव्यों को आत्मसात करके, नागरिकों में नैतिक दायित्व और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है , जो कानूनी अनुपालन से कहीं आगे जाती है। ये दैनिक जीवन में आचरण के लिए नैतिक मानदंड के रूप में कार्य करते हैं , लोकतांत्रिक आदर्शों, न्याय और राष्ट्रीय अखंडता को सुदृढ़ करते हैं।
इस प्रकार, मौलिक कर्तव्य कानून और नैतिकता के बीच एक सेतु का काम करते हैं , नागरिकों को जिम्मेदारी से कार्य करने, सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने और राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान देने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।